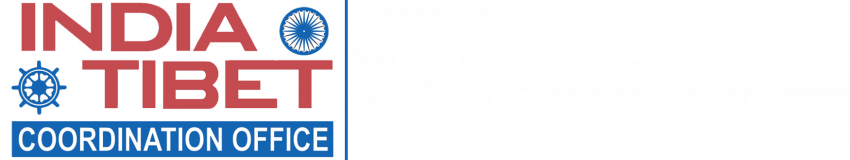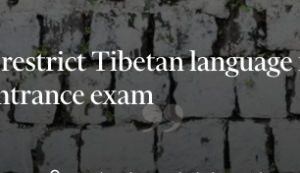अरुणाचल प्रदेश के पास यारलुंग सांगपो पर चीन के विशाल बांध के कारण बदले हुए जल प्रवाह से भारत, भूटान और बांग्लादेश को भू-राजनीतिक जोखिमों का खतरा है। इस तरह पानी रणनीतिक हथियार बन सकता है।
– बॉर्डरलेंस में सावांग दोरजी जेशोंग और कलसांग डोल्मा
०२ अगस्त २०२५
यारलुंग सांगपो के निचले क्षेत्र में चीन द्वारा बनाया जा रहा विशाल बांध हिमालय के भू-राजनीतिक परिदृश्य को बदल रहा है, जिससे तिब्बत से निकलनेवाले इस नद को लेकर दक्षिण एशिया के विरुद्ध चीन का जल-युद्ध और तेज हो रहा है। अगर हिमालय को लेकर चीन और भारत के बीच युद्ध होता है, तो पूर्वी हिमालय अगला युद्धक्षेत्र होगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि चीनी अधिकारी तिब्बत में यारलुंग सांगपो पर जलविद्युत बांधों के रूप में एक जल-बम बना रहे हैं। इसके भारत, भूटान और बांग्लादेश पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं।
सीमा पार जल संसाधनों पर नियंत्रण की चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को उजागर करने वाले एक कदम में, बीजिंग ने पिछले साल दिसंबर में घोषित अपनी १४वीं पंचवर्षीय योजना में यारलुंग सांगपो पर एक विशाल जलविद्युत बांध के निर्माण को औपचारिक रूप से शामिल किया है। १९ जुलाई को चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने तिब्बत के न्यिंगची शहर में नदी के निचले इलाकों में बांध के निर्माण की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के बगल में स्थित है।
इस परियोजना के दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत केंद्र बनने की उम्मीद है, जिसका अनुमानित वार्षिक उत्पादन ३०० अरब किलोवाट-प्रतिघंटे बिजली है, जो थ्री गॉर्जेस बांध से तीन गुना बड़ा है। यह बांध यारलुंग सांगपो के दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश से ठीक पहले नद के निचले हिस्से में बनाया जा रहा है, जहां यह ग्रेट बेंड पर यू-टर्न लेता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। यही पर यह ब्रह्मपुत्र नद बन जाता है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ली ने चाइना याजियांग ग्रुप का भी परिचय कराया, जो एक नव स्थापित सरकारी उद्यम है। इसे ही बांध के विकास की देखरेख का काम सौंपा गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत कम से कम १७० अरब डॉलर है और इसमें न्यिंगची के चारों ओर पांच जलप्रपात बांधों का निर्माण शामिल होगा। रिपोर्टों से पता चलता है कि इंजीनियर नद के कुछ मोड़ों को सीधा करने और प्रवाह एवं बिजली उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए सुरंगों के माध्यम से पानी की दिशा मोड़ने की योजना बना रहे हैं।
इस वर्ष की शुरुआत में चीन के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग ने भी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस को सौंपी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बांध और हांगकांग क्षेत्र से जुड़ी एक संबंधित बिजली पारेषण लाइन को शामिल किया था, जिसमें परियोजना के राष्ट्रीय रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया गया था।
परियोजना के स्थान ने भूकंपीय रूप से सक्रिय हिमालयी क्षेत्र में चिंता पैदा कर दी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि किसी बड़े भूकंप से अगर बांध के ढांचे को नुकसान होता है, तो यह निचले तटवर्ती क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनेगा। पर्यावरणविदों और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों ने भी पारिस्थितिकीय प्रभाव और प्रभावित होनेवाले निचले क्षेत्र देशों के साथ परामर्श न किये जाने पर चिंता जताई है।
चीन का दावा है कि यारलुंग सांगपो जलविद्युत परियोजना उसकी ‘पश्चिम से पूर्व विद्युत हस्तांतरण परियोजना (西电东送, जिडियन डोंगसोंग)’ का हिस्सा है, जो संसाधन संपन्न पश्चिमी क्षेत्रों में उत्पादित बिजली को औद्योगिक और घनी आबादी वाले पूर्वी प्रांतों में भेजने की दीर्घकालिक राष्ट्रीय रणनीति है। लेकिन उस हरित, तकनीकी भाषा के पीछे जल नियंत्रण, क्षेत्रीय प्रभाव और सीमा पर दावे से जुड़ी रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं छिपी हैं।
यह परियोजना चीन की व्यापक बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के अनुरूप है और यह क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में बीजिंग की बढ़ती दृढ़ता को दर्शाती है। भारतीय सीमा से केवल ३० किमी दूर तिब्बत के रणनीतिक रूप से संवेदनशील मेडोग क्षेत्र में स्थित यह परियोजना इस बात पर प्रकाश डालती है कि समकालीन भू-राजनीति में बुनियादी ढांचे का उपयोग शासन कला के एक साधन के रूप में कैसे तेजी से किया जा रहा है।
यारलुंग सांगपो नद तिब्बत से निकलता है और भारत से होते हुए बांग्लादेश में समुद्र में मिल जाता है। इसे भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सीमा पार के किसी भी ऊपरी इलाके के देश द्वारा किया गया एकतरफा हस्तक्षेप, जैसे कि बांध निर्माण, जल प्रवाह में बदलाव, कृषि को खतरे में डालकर और पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़कर, निचले इलाके के देशों को सीधे प्रभावित करता है। पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा, ऐसा नियंत्रण चीन को भारत और बांग्लादेश पर महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक लाभ भी देता है, जिससे जल क्षेत्रीय कूटनीति और सुरक्षा में रणनीतिक प्रभाव का एक संभावित साधन बन जाता है।
जब बीजिंग ने पिछले दिसंबर में बांध परियोजना की औपचारिक घोषणा की, तो भारत और बांग्लादेश दोनों ने इसके संभावित डाउनस्ट्रीम प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। जनवरी तक, भारत के विदेश मंत्रालय ने बीजिंग के साथ आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे को उठाया था। ‘चीनी पक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि ब्रह्मपुत्र के अपस्ट्रीम क्षेत्रों में गतिविधियों से डाउनस्ट्रीम राज्यों के हितों को नुकसान न पहुंचे।’
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने हाल ही में इस परियोजना को एक ‘वॉटर बम’ बताया था, और स्थानीय जनजातियों और आजीविका के लिए संभावित खतरे की चेतावनी दी थी। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में संवाददाताओं से कहा था, ‘मुद्दा यह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता… यह काफी गंभीर है, क्योंकि चीन इसका इस्तेमाल एक तरह के ‘वॉटर बम’ के रूप में भी कर सकता है।’
ये चिंताएं नई नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक- लोवी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि तिब्बती पठार से निकलने वाली नदियों पर नियंत्रण, चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभावी रूप से ‘दबाव’ डालने का मौका देता है, जिससे पानी के रणनीतिक हथियार बनने की आशंकाएं और प्रबल हो जाती हैं।
चीन द्वारा यारलुंग सांगपो बांध का शिलान्यास करने के ठीक एक दिन बाद अरुणाचल प्रदेश के मंत्री ओजिंग तासिंग ने कहा, ‘चीन ने पहले ही अपना बांध निर्माण शुरू कर दिया है और हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें कार्रवाई करनी होगी और हम कार्रवाई कर रहे हैं। यह भारत की भविष्य की जल सुरक्षा के बारे में है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है।’
यारलुंग सांगपो बांध परियोजना, तिब्बत में चीन के बुनियादी ढांचे के निर्माण के पीछे की गहरी राजनीतिक चाल को उजागर करती है। यह परियोजना विशुद्ध रूप से विकासात्मक या पर्यावरणीय पहल होने से कहीं अधिक क्षेत्र में अपने अधिकार और क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की बीजिंग की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि चीनी अधिकारियों ने यह खुलासा नहीं किया है कि कितने लोग विस्थापित हो सकते हैं, फिर भी स्पष्ट है कि तिब्बती समुदायों को स्थायी रूप से पुनर्वास का सामना करना पड़ रहा है, जो ‘आधुनिकीकरण’ की आड़ में जबरन पुनर्वास के पुराने तरीकों की याद दिलाता है। इन जबरन विस्थापनों के परिणामस्वरूप अक्सर पैतृक भूमि, सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक आजीविका का नुकसान होता है। इससे चीनी शासन के तहत तिब्बतियों द्वारा अनुभव किए गए ऐतिहासिक हाशिए पर रहने की विभीषिका और भी भीषण हो जाती है।
बीजिंग अपने क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास के अपने संप्रभु अधिकार का दावा करता है और इस परियोजना को एक हरित ऊर्जा पहल के रूप में प्रस्तुत करता है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, प्रदूषण में कमी लाएगी और ग्रामीण तिब्बतियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी। चीनी सरकारी मीडिया अक्सर इन विशाल बांधों को विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए ‘दोनों पक्षों की जीत’ वाला बताता है। हालांकि, चीन के इस कथन को तिब्बती विद्वान और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक गलत बताते हैं। वे इस परियोजना को एक अत्यंत संवेदनशील सीमांत क्षेत्र में संसाधन दोहन और राजनीतिक दमन के अकाट्य हथियार के रूप में देखते हैं।
राजनीतिक रूप से चीन यारलुंग सांगपो परियोजना को लेकर इस क्षेत्र और उसके बाहर अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक योजना बना रहा है।
नद पर नियंत्रण करके चीन तिब्बत के पानी का उपयोग भारत के खिलाफ जल युद्ध के लिए कर रहा है। इस मामले में यह बांध न केवल एक ऊर्जा अवसंरचना बन जाता है, बल्कि दक्षिण एशिया में चीन की भू-राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए रणनीतिक हथियार भी बन जाता है।